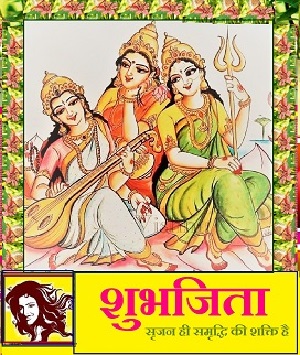सभी सखियों को नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे देश में स्त्री- पुरुष अनुपात के आंकड़े समान नहीं है और इस असमानता के पीछे एक लंबी परंपरा तो नहीं कहूंगी लेकिन सजिश जरूर काम कर रही है। और उसी की वजह से, आज इक्कीसवीं शताब्दी में भी बहुत से पढ़े- लिखे माता -पिता भी यह मानते हैं कि बेटे को जन्म दिए बिना उन्हें इहलोक और परलोक दोनों में मुक्ति नहीं मिल सकती। बेटों को ही जीवन का असली धन मानने वाले पुरुष-सत्तात्मक समाज ने बेटों की चाह में बेटियों के आने का रास्ता हमेशा ही बंद किया। जो समाज स्त्री पुरुष के समान सहयोग ही नहीं सह अस्तित्व पर कायम था और सहज स्वाभाविक रूप से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा था, उसमें कब और कैसे स्त्रियां अनचाही बन गयीं और उन्हें समाप्त कर देने की दुर्भावना हमारे मन में पनपने लगी, इसका पता ही न चला। निश्चित रूप से यह आदिम युग में नहीं ही हुआ होगा। लेकिन जैसे- जैसे मनुष्य ने सभ्यता का लिहाफ ओढ़ा, वह और ज्यादा बनैला हो गया। विकास के किस क्रम में लड़कियों को बोझ समझा जाने लगा इसके बारे में हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि विवाह संस्था की स्थापना के कुछ समय बाद लड़कियों के विवाह के लिए ढ़ेरों दहेज की आवश्यकता पड़ने लगी होगी, वह मोड़ सभ्यता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए ठीक किस समय आया, इसका अनुमान भर लगाया जा सकता है। हालांकि कई ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माता- पिता अपनी बेटी की नई गृहस्थी के लिए भेंट स्वरूप कुछ सामान दिया करते थे ताकि वह अपने नये जीवन का आरंभ कर सके लेकिन वह कब जबरिया मांग में बदल गया, इसकी भी महज परिकल्पना ही की जा सकती है।
लड़कियों को बोझ समझने का एक सिरा संपत्ति के विभाजन से भी जुड़ता है। जब मनुष्य के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती थी तब बेटे और बेटी के बीच में अधिक अंतर नहीं रहा होगा लेकिन जिस स्थिति में विवाह के पश्चात संपत्ति विभाजन का प्रश्न सामने आया होगा तभी बेटियों को पराया धन आदि सिद्ध करने के लिए कई तर्क गढ़े गये होंगे और धर्मशास्त्र आदि लिखे गए होंगे जिसमें कन्या दाय से मुक्त होने के महत्त्व को बढ़ा चढ़ाकर सिद्ध किया गया होगा। उसी समय स्वर्ग नरक आदि की परिकल्पना करते हुए यह सिद्ध करने की कोशिश भी हुई होगी कि पिता की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसे बेटा मुखाग्नि देगा और उसका श्राद्ध कर्म करेगा। स्त्रियों को कोमलांगी सिद्ध करते हुए उन स्थानों से दूर रखा गया जहां पार्थिव शरीर का संस्कार किया जाता था, शायद इसीलिए आज के समय में भी समाज के एक बड़े हिस्से में स्त्रियों का शमशान जाना उचित नहीं समझा जाता है। आप कल्पना कीजिए कि सभ्यता के आदिम चरण में जो स्त्रियां श्रमपूर्वक शिकार करती थीं और अपनी रक्षा करने में सक्षम थीं, वे ही सभ्य समाज में रक्षणीया समझी गईं और उनका किसी ना किसी पुरुष के संरक्षण में रहना आवश्यक बना दिया गया। युवावस्था में अपने लिए साथी को चयनित करने का अधिकार भी उसके पास नहीं रहा जो कि कबीलाई संस्कृति में हुआ करता था। हालांकि उस संस्कृति में एक कबीले विशेष के शक्ति संपन्न युवा द्वारा दूसरे कबीले की युवती की हरण भी किया जाता था और प्रतिरोध करने पर उसके कुटुंब जनों की हत्या भी कर दी जाती थी। अपहरण और हत्या के इन्हीं सिलसिलों के कारण संभवतः कबीले के लोग अपनी -अपनी पुत्रियों की रक्षा के लिए तत्पर हो उठे होंगे और इसी क्रम में बेटियों के विवाह आदि को परिवारों के सम्मान के साथ जोड़ दिया गया होगा और उसके लिए वर चुनने या उसे सुपात्र के हाथों सौंपने का अधिकार पिता या परिवार के मुखिया ने अपने पास रखा। जब कन्या दाय एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई तभी संभवतः दहेज प्रथा का जन्म हुआ होगा जिसने कालांतर में इतना विकराल रूप ले लिया कि माता- पिता बेटी के विवाह को संपन्न करने के लिए बर्बादी के कगार तक आ गये।
लब्बोलुआब यह है कि परिवार के सम्मान का सवाल और दहेज के मसलों ने क्रमशः पुत्रियों को पिता और परिवार के लिए बोझ में परिवर्तित कर दिया और सभ्यता के विकास में वह अमानवीय समय भी आया जब बेटियों से मुक्ति की कामना ही नहीं की जाने लगी बल्कि उनसे मुक्ति पाने के लिए जन्म के तुरंत बाद उनकी हत्या भी की जाने लगी। बाद में तकनीकी विकास और मनुष्य की अर्थ लिप्सा के कारण बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाने लगा जिसका सिलसिला अब भी निरंतर जारी है। और इस सिलसिले ने ही समाज में स्त्री- पुरुष अनुपात को बिगाड़ दिया है। बहुत से प्रांत ऐसे हैं जहां बेटों के विवाह के लिए लड़कियां नहीं मिलती और देश के दूसरे हिस्सों से जहां यह अनुपात अब भी सही है, से लड़कियों को खरीद कर लाया जाता है। लेकिन इस गलत अनुपात को सही करने की चिंता शायद अब भी हमें नहीं है। आज भी अधिकांश दंपति पुत्र-रत्न की प्राप्ति की कामना करते हैं क्योंकि बेटी तो पराया धन ही मानी जाती है और संपत्ति का वारिस तो बेटा ही हो सकता है तथा माता-पिता की अंत्येष्टि का अधिकार भी उसी के पास सुरक्षित हैं। इन्हीं मान्यताओं के कारण बेटियों की मां को संतानवती होने के बावजूद बांझ कह कर पुकारा जाता है और किसी तथाकथित शुभ कार्य में उसे शामिल करने से यथासंभव परहेज किया जाता है। और इसी संकीर्ण सोच के कारण समाज के कुछ तथाकथित सभ्य लोग बेटों की चाह में बेटियों को कोख में ही मार देते हैं तो कुछ बेटे की प्रतीक्षा में बेटियों की लाइन लगा देते हैं। मैत्रेयी पुष्पा की कहानी “तुम किसकी हो बिन्नी” में इस कटु यथार्थ को मार्मिकता से उकेरा गया है।
सखियों, इस तरह के दृश्य आज भी अगर आम हैं तो हमें थोड़ा ठहर कर सोचने की आवश्यकता है कि आखिर कब तक हम इन संकीर्ण रूढ़ियों का शिकार होकर बेटियों का तिरस्कार करते रहेंगे या फिर उनकी बलि चढ़ाते रहेंगे। विकास के बड़े -बड़े दावों के बावजूद हम मानसिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार हैं जिससे मुक्त हुए बिना ना समाज का समग्र विकास संभव हो पाएगा ना ही देश का। बेटियों को बचाने और पढ़ाने के नारे लगाने और पोस्टर चिपकाने भर से स्थितियां नहीं बदलेंगी। स्थितियों को बदलने के लिए हमें अपने मानस को बदलना होगा। आप स्वयं भी इस बारे में सोचिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए।
आज, विदा सखियों। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी लेकिन तब तक आप इस मुद्दे पर सोचिए जरूर और औरों को भी सोचने के लिए कहिए।